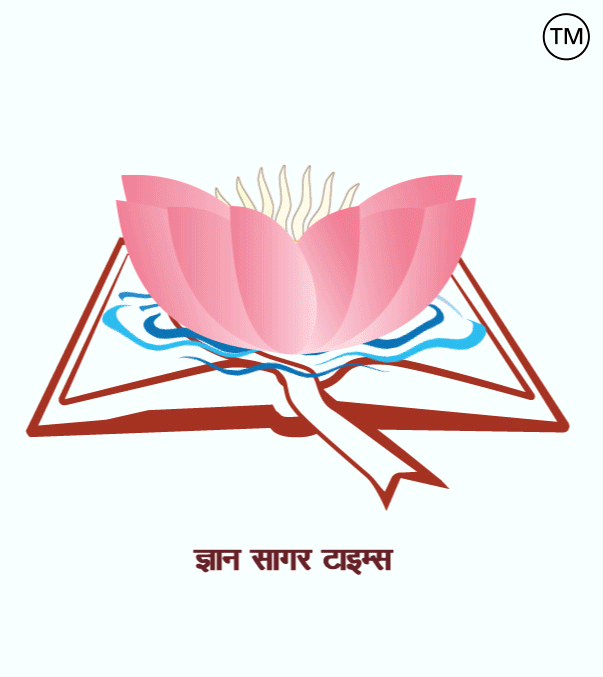हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संक्रांति आ ही गई. आज के बाद भगवान भास्कर उत्तरायण हो जायेंगें. अब धीरे-धीरे हेमंत ऋतू या यूँ कहें कि भीषण ठंड से निजात मिलने के दिन आ रहें हैं. आखिर संक्रांति के बाद ही क्यूँ हेमंत ऋतू समाप्त होता है. आखिर क्या कारण है कि प्रति वर्ष 14-15 जनवरी के बाद ही मौसम का मिजाज ठीक होता है साथ ही यह भी जानते हैं कि इस समय को मकर संक्रांति क्यों कहते है और इसका महत्व क्या है?
बताते चलें कि, संक्राति का अर्थ होता है सूर्य के एक राशि से दुसरे राशि में प्रवेश करना या यूँ कहें कि, एक राशि से दुसरे राशि में गमन करना. यह ज्योतिषीय गणना अनुसार प्रति वर्ष 14-15 जनवरी को पड़ता है. हम सभी जानते हैं कि, पृथ्वी की परिक्रमापथ जो अंडाकार है उसे 360 अंशों में 30-30 अंशों के समूह में 12 राशियों में विभाजित किया गया है. ज्ञात है कि, 365 दिन 6 घंटे का एक साल होता है जबकि, चन्द्र वर्ष 354 दिनों का होता है चुकीं, चन्द्रमा में परिवर्तन होता ही रहता है, इसिलिय चन्द्रवर्ष निश्चित नहीं होता है. इसी परिवर्तन के कारण हर चार सालों में फरवरी 29 दिनों का होता है. सूर्य के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने की अवधि को दक्षिणायन तथा दक्षिण से उत्तर की ओर के जाने को उत्तरायण कहते हैं.
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, संक्रमण पर्व मकर संक्रान्ति में मकर का विशेष महत्व बताया गया है. इसकी अलग तरह से विवेचना की गई है. चुकीं मकर मत्स्य वर्ग में आता है और माँ गंगा का वाहन भी है और गंगा को मकरवाहिनी भी कहते है. वायुपुराण के अनुसार, मकर को नौ निधियां भी कहते हैं. ये नौ निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द नील और खर्व. पृथ्वी की एक अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं जबकि, ज्योतिष गणना के बारह राशियों में से दसवीं राशि का नाम मकर है. श्रीमद्भागवत के अनुसार, सुमेरु पर्वत के उत्तर में दो पर्वत हैं उनमें से एक का नाम मकर पर्वत भी है. पुरानों के अनुसार, कामदेव की पताका का प्रतीक होता है मकर इसीलिए, कामदेव को मकरध्वज भी कहा जाता है.
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, सूर्य के दक्षिण से ऊर्ध्वमुखी होकर उत्तरस्थ होने की वेला को संक्रान्ति पर्व के रूप में स्वीकार किया गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार महात्मा भीष्म की इच्छामृत्यु वाली घटना भी इसके महत्व एवं महिमा को भी प्रकाशित करती है. महाभारत पुराण में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि, शर–शैय्या पर पड़े गंगापुत्र भीष्म से दर्शन करने आये ऋषियों से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने शरीर-त्याग करने का संकल्प दुहराते हैं वहीँ, शिव पुराण के अनुसार, उत्तरायण एवं मकर संक्रान्ति के अवसर पर हवन-पूजा, खान-पान में तिल एवं तिल से बनी वस्तुओं पर अधिक जोर दिया गया है. सूर्य जब उत्तरी गोलार्द्ध में रहता है तब रवी की फसल चना, गेहूं आदि फसल पकने की स्थिति में होती है. इस समय सूर्य के ताप से उन फसलों को बढ़ने और पकने में सहायता मिलती है. यही कारण है कि मकर संक्रान्ति के लोकपर्व पर लोग अन्य को सूर्य भगवान को अर्पित करते है. लोक व्यवहार में भी तिल-खिचड़ी आदि गर्म पदार्थों के सेवन पर विशेष जोर दिया जाता है. जबकि हमारे ऋषियों ने सुखी जीवन के लिए अनेकानेक विधाओं का उल्लेख किया है उसमे नदी स्नान का विशेष महत्व दिया गया है. ज्ञात है कि, नदियों के उद्गम स्थान पर्वत होते हैं, जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं और आप जानते ही हैं कि इन पर्वतों पर दिव्य औषधियाँ भी फलती-फूलती हैं उनमे वर्षा के जल में मिलकर नदियों में गिरती हैं और उन नदी के पानी में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है. इन्ही कारणों से पुरानों में नदी स्नान पर जोड़ दिया गया है.
वैज्ञानिक सत्य है कि उत्तरायण में सूर्य का ताप शीत के प्रकोप को कम करता है वहीं, पुराणकारों ने भी मकर संक्रान्ति को सूर्य उपासना का विशिष्ट पर्व माना है. इस अवसर पर भगवान सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र के साथ पूजा-उपासना, यज्ञ-हवन का अलौकिक महत्व होता है. आयुर्वेद के जानकारों के अनुसार, शीतकालीन ठण्डी हवा शरीर में अनेक रोगों को जन्म देती है. चरक संहिता के अनुसार, इस मौसम में घी-तेल, तिल-गुड़, गन्ना, धूप और गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए.
पुरानों के अनुसार तिल के 6 प्रकार के उपयोग बताये गये हैं. ये उपाय… तिल मिश्रित स्नान, तिल का उबटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल, तिल का हवन और तिल का भोजन. कहा जाता है कि, तिल समस्त रोगों का नाश करता है जबकि, तिल स्नेह का और गुड मिठास का प्रतीक माना जाता है. महाभारत पुराण के अनुसार, संक्राति के अवसर पर तिल दान एवं तिल खाने की बात को स्वीकार किया गया है. उसके बाद से ही पुरे भारत वर्ष में मकर संक्रांति के अवसर पर तिल खाने और दान करने की परम्परा चली आ रही है. यह संस्कृति चुकीं महाभारत काल की आस्था, पौराणिक जन-विश्वास प्राकृतिक निधि, जलदेवता, वरुणा तथा गंगा वाहन मकर से जुड़ा हुआ है और सूर्य-रश्मियों के क्रान्तिकारी उत्कर्ष से भरा है और संक्रान्ति के अवसर पर गायत्री महामंत्र से सूर्योपासना का संदेश छुपा हुआ होता है.
========== ========= ===========
Makar Sankranti…

Like every year, Sankranti has arrived this year too. After today Lord Bhaskar will become Uttarayan. Now gradually Hemant Ritu or rather the days of getting relief from the severe cold are coming. After all, why does Hemant Ritu end only after Sankranti? After all, what is the reason that the weather becomes better only after 14-15 January every year? Also do we know why this time is called Makar Sankranti and what is its significance?
Let us tell you that Sankranti means the Sun entering from one zodiac sign to another or in other words, moving from one zodiac sign to another. According to astrological calculations it falls on 14-15 January every year. We all know that the Earth’s orbit, which is oval, is divided into 12 zodiac signs in groups of 30 each in 360 degrees. It is known that a year is of 365 days and 6 hours, whereas, the lunar year is of 354 days, the moon keeps changing, hence the lunar year is not fixed. Due to this change, every four years February has 29 days. The period of Sun’s movement from north to south is called Dakshinayan and its movement from south to north is called Uttarayan.
According to mythological texts, the special importance of Makar has been mentioned in the transition festival Makar Sankranti. It has been discussed in different ways. Because Makar comes in the Pisces category and is also the vehicle of Mother Ganga and Ganga is also called Makarvahini. According to Vayupuran, Capricorn is also called nine Nidhis. These nine treasures are Padma, Mahapadma, Shankha, Makara, Kachhapa, Mukunda, Kund Neel and Kharva. A latitude line of the Earth is called the Tropic of Capricorn, while the name of the tenth zodiac sign out of the twelve zodiac signs of astrological calculation is Capricorn. According to Srimad Bhagwat, there are two mountains to the north of Sumeru Mountain; one of them is also named Makar Mountain. According to the ancients, the symbol of Kamadeva’s flag is Capricorn, that is why Kamadeva is also called Makardhwaj.
According to mythological texts, the time when the Sun turns from south to north has been accepted as the festival of Sankranti. According to mythology, the incident of euthanasia of Mahatma Bhishma also highlights its importance and glory. There is a clear mention of the fact in the Mahabharata Purana that Ganga’s son Bhishma, lying on his bed, reiterates to the sages who came to visit him to give up his body on the day of Uttarayan of the Sun. Whereas, according to Shiv Puran, on the days of Uttarayan and Makar Sankranti, On the occasion of havan-puja, more emphasis has been given on sesame seeds and items made from sesame seeds in food and drink. When the Sun remains in the Northern Hemisphere, Ravi crops like gram, wheat etc. are at the stage of ripening. At this time, the heat of the sun helps those crops to grow and ripen. This is the reason why on the folk festival of Makar Sankranti, people offer other things to the Sun God. Even in public practice, special emphasis is given on consumption of hot items like sesame seeds, khichdi etc. While our sages have mentioned many methods for a happy life, special importance has been given to river bathing. It is known that the origin places of rivers are mountains, from where these rivers originate and you know that divine medicines also flourish on these mountains, they mix with the rain water and fall into the rivers and in the water of those rivers. The importance of bathing increases even more. For these reasons, river bathing has been added to the Puranas.
It is a scientific truth that the heat of the Sun in Uttarayan reduces the severity of cold, whereas the Purankars have also considered Makar Sankranti as a special festival of Sun worship. On this occasion, worship of Lord Surya along with Gayatri Mantra and Yajna-Havan have supernatural significance. According to Ayurveda experts, cold winter air gives rise to many diseases in the body. According to Charak Samhita, ghee-oil, sesame-jaggery, sugarcane, incense and hot water should be used in this season.
According to the ancients, 6 types of uses of sesame have been described. These remedies… bath mixed with sesame seeds, boiling of sesame seeds, tilak made of sesame seeds, water mixed with sesame seeds, havan made with sesame seeds and food made with sesame seeds. It is said that sesame destroys all diseases whereas sesame is considered a symbol of love and jaggery is considered a symbol of sweetness. According to Mahabharata Purana, donating sesame seeds and eating sesame seeds on the occasion of Sankranti has been accepted. Since then, the tradition of eating and donating sesame seeds on the occasion of Makar Sankranti has been going on throughout India. This culture is associated with the faith of the Mahabharata period, mythological public belief, natural wealth, water god, Varuna and Ganga vehicle Makar and is full of revolutionary exaltation of sun rays and on the occasion of Sankranti, the message of Surya worshi.