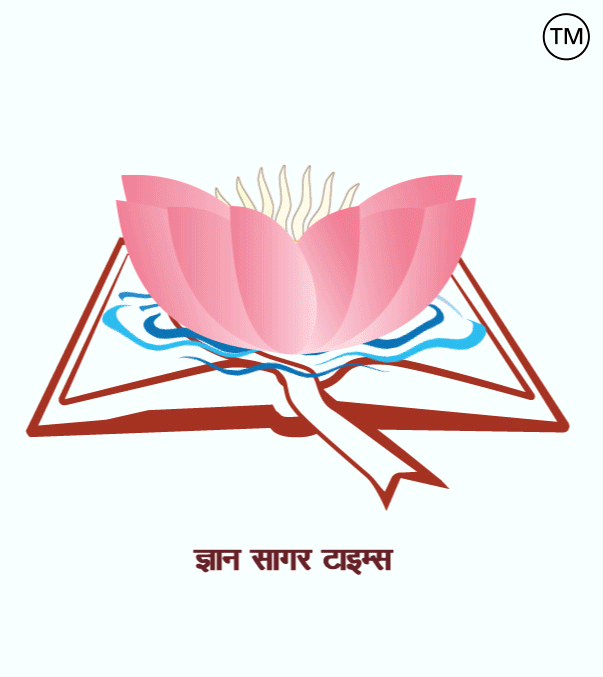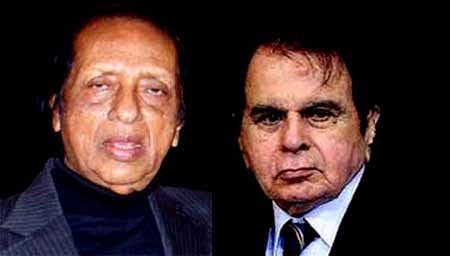
व्यक्ति विशेष– 558.
सिक्खों के आठवें गुरु गुरु हर किशन सिंह
गुरु हर किशन सिंह जी सिक्खों के आठवें गुरु थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब, पंजाब में हुआ था. वे गुरु हर राय जी और माता किशन कौर के छोटे पुत्र थे. गुरु हर किशन सिंह को उनके पिता ने 7 अक्टूबर 1661 को गुरु की गद्दी पर बैठाया.
गुरु हर किशन सिंह की उम्र बहुत छोटी थी जब उन्होंने गुरु का पद संभाला, लेकिन उनकी महानता और आध्यात्मिकता ने सिक्ख समुदाय को बहुत प्रभावित किया. वे दया, सेवा, और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं. दिल्ली में चेचक की महामारी के दौरान, उन्होंने बीमार लोगों की सेवा की और उन्हें सांत्वना दी.
उनकी सेवा के कारण वे स्वयं भी चेचक से संक्रमित हो गए और 30 मार्च 1664 को उनका निधन हो गया. उनकी समाधि दिल्ली में बाला साहिब गुरुद्वारे में स्थित है. गुरु हर किशन सिंह की स्मृति सिक्ख धर्म में विशेष स्थान रखती है, और वे बच्चों के संरक्षक संत के रूप में माने जाते हैं. गुरु हर किशन सिंह जी का जीवनकाल भले ही बहुत छोटा रहा हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया सेवा और त्याग का मार्ग सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा.
========== ========= ===========
स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतउल्ला
मोहम्मद बरकतउल्ला, जिन्हें बरकतउल्ला भोपाली के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे. उनका जन्म 7 जुलाई 1854 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था. उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया. बरकतउल्ला भोपाली का प्रारंभिक जीवन भोपाल में बीता, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की. बाद में, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों से संपर्क स्थापित किया. वे स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित विद्रोह के समर्थक बन गए.
बरकतउल्ला ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास किया. वे 1900 की शुरुआत में इंग्लैंड में “इंडियन होमरूल सोसाइटी” में शामिल हुए और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार के लिए यूरोप और अमेरिका के कई देशों में सक्रिय रूप से काम किया. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्थन प्राप्त करने के लिए कई देशों के नेताओं से संपर्क साधा. मोहम्मद बरकतउल्ला गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में से एक थे, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चला रही थी. गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका में था, और इसका उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था. बरकतउल्ला ने इस पार्टी के साथ मिलकर अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने का काम किया.
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मोहम्मद बरकतउल्ला ने अफगानिस्तान में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह सरकार वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में राजा अमानुल्लाह खान के समर्थन से स्थापित की गई थी. इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रपति और बरकतउल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था. इस सरकार का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में विद्रोह को संगठित करना था. बरकतउल्ला एक प्रखर लेखक और पत्रकार भी थे. उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों का प्रचार किया. वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तीखी आलोचना करते थे और भारतीय समाज में स्वाधीनता और स्वाभिमान की भावना को जागृत करने के लिए काम करते थे. उन्होंने कई अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखे, जिनमें “अल-हिलाल” और “गदर” जैसे पत्र प्रमुख थे.
बरकतउल्ला ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जर्मनी, तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों से समर्थन जुटाने का काम किया. उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा. मोहम्मद बरकतउल्ला का निधन 20 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ. वे ब्रिटिश शासन के कारण अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारत लौट नहीं सके, लेकिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जीवन समर्पित कर दिया.
मोहम्मद बरकतउल्ला भोपाली का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन क्रांतिकारियों में गिना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के भीतर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आजादी की अलख जगाई. उनकी याद में भोपाल में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो उनके सम्मान में है और उनके योगदान को याद दिलाता है.
========== ========= ===========
साहित्यकार चन्द्रधर शर्मा गुलेरी
चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ हिंदी साहित्य के लेखक, आलोचक और निबंधकार थे. उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था. वे अपनी कहानियों और निबंधों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं. उनका लेखन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. गुलेरी जी ने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में गहरी शिक्षा प्राप्त की थी. वे पेशे से प्रोफेसर थे और उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया. इसके अलावा, वे एक प्रभावशाली वक्ता और विचारक भी थे.
प्रमुख कृतियाँ: –
उसने कहा था: – यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसे हिंदी साहित्य की सबसे उत्कृष्ट कहानियों में से एक माना जाता है. इस कहानी में प्रेम, त्याग और बलिदान के विषयों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है.
सुखमय जीवन: – यह एक निबंध संग्रह है जिसमें गुलेरी जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं.
चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ ने हिंदी साहित्य में अपनी सशक्त लेखनी से महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी कहानियों और निबंधों में समाज के विविध पहलुओं, मानवीय भावनाओं और संस्कृति की झलक मिलती है. उनकी लेखनी में सरलता और प्रवाह था, जो पाठकों को सीधे प्रभावित करता था.
चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ का निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था. वे मात्र 39 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अपने छोटे से जीवनकाल में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल्य रचनाएँ दीं. चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ की साहित्यिक धरोहर आज भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उनकी रचनाएँ आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं.
========== ========= ===========
संगीतकार अनिल बिस्वास
अनिल बिस्वास भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित संगीतकार और गायक थे. उनका जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल (अब बांग्लादेश में) में हुआ था. वे हिंदी सिनेमा में वर्ष 1940 – 50 के दशक के प्रमुख संगीत निर्देशकों में से एक थे और उनके द्वारा रचित संगीत ने उस समय के भारतीय फिल्म संगीत को नई दिशा दी.
अनिल बिस्वास ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1930 के दशक में की. वे हिंदी सिनेमा के पहले संगीतकारों में से थे जिन्होंने फिल्म संगीत में ऑर्केस्ट्रा और विविधता लाने की पहल की. उनके संगीत में शास्त्रीय और लोक संगीत का समन्वय था.
प्रमुख फिल्में: –
किस्मत (1943): – इस फिल्म का संगीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ, खासकर “दो हंसों का जोड़ा” गीत.
आरजू (1950): – इस फिल्म का संगीत भी बहुत सराहा गया.
तराना (1951): – मधुबाला और दिलीप कुमार अभिनीत इस फिल्म के गाने भी काफी प्रसिद्ध हुए.
अनारकली (1953): – इस फिल्म का संगीत भी बहुत ही लोकप्रिय रहा.
अनिल बिस्वास ने फिल्मी संगीत में अनेक प्रयोग किए और उसे एक नई ऊँचाई तक पहुँचाया. उनके संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और आधुनिक संगीत का संगम होता था. उन्होंने कई गायकों को फिल्म उद्योग में स्थापित किया, जिनमें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी शामिल हैं.
अनिल बिस्वास का योगदान भारतीय फिल्म संगीत में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. उन्होंने संगीत निर्देशन में नई तकनीकों और साज-सज्जा का प्रयोग किया और हिंदी फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया. उनके योगदान के कारण ही वे “भजन सम्राट” के नाम से भी जाने जाते हैं. अनिल बिस्वास का निधन 31 मई 2003 को नई दिल्ली में हुआ था. उनकी संगीत यात्रा और योगदान को भारतीय सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा.
अनिल बिस्वास की संगीत यात्रा ने भारतीय फिल्म संगीत को समृद्ध किया और उनके योगदान को सदैव सराहा जाएगा.
========== ========= ===========
अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य
अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता थे. उनका जन्म 7 जुलाई 1922 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था. चंद्रशेखर वैद्य को विशेष रूप से वर्ष 1960 – 70 के दशक की हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है.
चंद्रशेखर ने वर्ष 1947 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की. उनकी प्रमुख फिल्में: – “चौदहवीं का चांद” (1960), “बूंद जो बन गई मोती” (1967), “विनाश” (1958) और कई अन्य हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और “चरणों की सौगंध” (1988) जैसी फिल्में बनाईं.
चंद्रशेखर वैद्य को रामानंद सागर की प्रसिद्ध टीवी श्रृंखला “रामायण” (वर्ष 1987-88) में “सुमंत” के किरदार के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है. सुमंत, महाराज दशरथ के मंत्री और राम के परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे. इस भूमिका ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया.
चंद्रशेखर का विवाह शोभा चंद्रशेखर से हुआ था, और उनके दो बेटे हैं. उनके परिवार ने भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है. चंद्रशेखर वैद्य का निधन 16 जून 2021 को 98 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ था. चंद्रशेखर वैद्य का योगदान भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में अविस्मरणीय है. उनके अभिनय, निर्देशन और विशेष रूप से “रामायण” में उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा.
========== ========= ===========
क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी
महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें आमतौर पर एम.एस. धोनी के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रसिद्ध और सफल क्रिकेटरों में से एक हैं. उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में हुआ था. धोनी अपनी कप्तानी, विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे महान कप्तानों में से एक माना जाता है. धोनी का जन्म रांची में हुआ और उन्होंने वहीं की डी.ए.वी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई की. धोनी ने अपने कैरियर की शुरुआत बिहार क्रिकेट टीम से की और बाद में झारखंड क्रिकेट टीम के लिए खेले. उनके प्रदर्शन ने जल्द ही चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा. धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया. उन्होंने 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया. धोनी ने 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया.
कप्तानी
धोनी के नेतृत्व में भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता. धोनी ने भारत को 28 साल बाद दूसरा वर्ल्ड कप जिताया. फाइनल में धोनी के नाबाद 91 रनों की पारी और विनिंग सिक्स आज भी यादगार है. धोनी के नेतृत्व में भारत ने यह ट्रॉफी भी जीती और सभी प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान बने.
आईपीएल
धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं. उनके नेतृत्व में CSK ने कई बार आईपीएल खिताब जीते हैं. धोनी ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा स्टंपिंग, एक दिवसीय और टी20 में सबसे ज्यादा छक्के, आदि. धोनी को कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म श्री और पद्म भूषण शामिल हैं. धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वे अभी भी आईपीएल में खेलते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तानी करते हैं. धोनी का विवाह साक्षी सिंह रावत से हुआ है और उनकी एक बेटी है, जिसका नाम जीवा है.
महेंद्र सिंह धोनी न केवल अपने खेल के लिए बल्कि अपने शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक सोच और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है.
========== ========= ===========
कैप्टन विक्रम बत्रा
कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के एक वीर और बहादुर अधिकारी थे, जिन्हें वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में अद्वितीय साहस और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ था. उनके पिता जी. एल. बत्रा एक शिक्षक थे और माता कमल कांता बत्रा एक स्कूल शिक्षक थी. विक्रम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डी.ए.वी पब्लिक स्कूल, पालमपुर से की और फिर डी.ए.वी कॉलेज, चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई की. उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), देहरादून से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया.
विक्रम बत्रा ने 6 दिसंबर 1997 को भारतीय सेना की 13वीं जम्मू और कश्मीर राइफल्स (13 JAK Rif) में कमीशन प्राप्त किया. वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, कैप्टन विक्रम बत्रा ने अदम्य साहस और नेतृत्व का परिचय दिया. उन्होंने प्वाइंट 5140 और प्वाइंट 4875 पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके अद्वितीय साहस और वीरता के लिए उन्हें “शेरशाह” के नाम से भी जाना जाता है. 7 जुलाई 1999 को, प्वाइंट 4875 पर कब्जा करने के दौरान कैप्टन बत्रा ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया. उनके अद्वितीय नेतृत्व और निडरता ने उनकी टीम को जीत दिलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश इस संघर्ष में वे वीरगति को प्राप्त हुए. कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.
कैप्टन विक्रम बत्रा एक दृढ़ निश्चयी और साहसी व्यक्ति थे. उनके परिवार, दोस्तों और साथी सैनिकों ने उन्हें एक अत्यंत प्रेरणादायक और निडर व्यक्ति के रूप में याद किया. कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता और बलिदान ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया है और वे आज भी भारतीय सेना के आदर्श और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं. उनके जीवन पर आधारित फिल्म “शेरशाह” (2021) में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनकी भूमिका निभाई, जिससे उनकी कहानी और वीरता को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में मदद मिली.
कैप्टन विक्रम बत्रा का बलिदान और उनकी वीरता भारतीय सेना और राष्ट्र के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा. उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा.
========== ========= ===========
शायर अब्दुल क़ावी देसनावी
अब्दुल क़ावी देसनावी एक प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर थे, जिनका जन्म 1 नवम्बर, 1930 को बिहार राज्य के नालन्दा ज़िले के देसना गाँव में हुआ था. वे अपने शेरों और गज़लों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें उन्होंने प्रेम, ज़िंदगी, समाजिक मुद्दों और इंसानियत की बातें की हैं. उनकी शायरी में गहराई और भावनाओं की एक विशेष मिठास होती है.
देसनावी की शायरी आमतौर पर सरल, सुगम और स्पष्ट होती है. वे शायरी में संवादात्मक और आम जीवन के अनुभवों को बखूबी शामिल करते हैं. उन्होंने उर्दू साहित्य को समृद्ध करने के लिए अनेक रचनाएँ की हैं. उनकी शायरी में न केवल प्यार का जज़्बा होता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी उनकी गहरी नजर होती है.
उनकी कई रचनाएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और उन्हें शायरी की महफिलों में भी विशेष पहचान मिली है. अब्दुल क़ावी देसनावी का योगदान उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण है, और उनकी रचनाएँ आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है. क़ावी देसनावी का निधन 7 जुलाई, 2011 को भोपाल में हुआ था.
========== ========= ===========
हिंदी और रूसी साहित्यकार मदन लाल मधु
मदन लाल मधु हिंदी और रूसी साहित्य के एक प्रमुख विद्वान थे. उन्होंने हिंदी और रूसी साहित्य के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया और दोनों भाषाओं में साहित्यिक कृतियों का अनुवाद और प्रचार-प्रसार किया. उनका जन्म 28 जुलाई 1925 को हुआ था और वे हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक थे.
मदन लाल मधु का जन्म पंजाब में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब से प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए रूस चले गए. वहां उन्होंने रूसी भाषा और साहित्य में गहरी पकड़ बनाई. मदन लाल मधु ने हिंदी और रूसी साहित्य के बीच पुल का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने रूसी साहित्य की अनेक महान कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी साहित्य को रूसी पाठकों के बीच लोकप्रिय बनाया.
प्रमुख कृतियाँ और अनुवाद: –
मदन लाल मधु ने लियो टॉल्स्टॉय, फ़्योडोर दोस्तोयेव्स्की, अलेक्जेंडर पुश्किन और कई अन्य प्रमुख रूसी लेखकों की रचनाओं का हिंदी भाषा में अनुवाद किया वहीं , उन्होंने प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और अन्य हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया. मधु ने अपने साहित्यिक करियर में कई मूल रचनाएँ भी लिखीं, जो हिंदी साहित्य के समृद्ध कोष का हिस्सा हैं.
मदन लाल मधु ने भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया. उन्होंने साहित्यिक गोष्ठियों, संगोष्ठियों और सेमिनारों के माध्यम से दोनों देशों के साहित्यकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया. मदन लाल मधु के योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले. उन्हें दोनों देशों में उनके साहित्यिक योगदान के लिए मान्यता दी गई.
मदन लाल मधु का निधन 11 जनवरी 2014 को हुआ था. उनके निधन से हिंदी और रूसी साहित्य को अपूरणीय क्षति हुई, लेकिन उनका योगदान और उनकी कृतियाँ आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच जीवित हैं. मदन लाल मधु के कार्यों ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी साहित्यिक धरोहर और दोनों भाषाओं के साहित्य में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा.
========== ========= ===========
अभिनेता दिलीप कुमार
दिलीप कुमार जिन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है, उनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था. उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, ब्रिटिश भारत (अब पाकिस्तान में) में हुआ था. वे भारतीय सिनेमा के “ट्रैजेडी किंग” के रूप में प्रसिद्ध थे और उनकी अभिनय कला ने हिंदी फिल्म उद्योग को एक नई दिशा दी.
दिलीप कुमार का जन्म पेशावर के एक पठान परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो एक फल व्यापारी थे. दिलीप कुमार की प्रारंभिक शिक्षा नासिक में हुई. परिवार के मुंबई (तब बॉम्बे) स्थानांतरित होने के बाद, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा मुंबई में पूरी की. दिलीप कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1944 में फिल्म “ज्वार भाटा” से की, जो एक औसत फिल्म थी. लेकिन उन्होंने अपने अभिनय कौशल से जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई.
फिल्में: –
अंदाज़ (1949): – राज कपूर और नरगिस के साथ यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई.
देवदास (1955): – बिमल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें “ट्रैजेडी किंग” का खिताब दिलाया.
नया दौर (1957): – यह फिल्म भी दिलीप कुमार के करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई.
मुगल-ए-आज़म (1960): – इस ऐतिहासिक फिल्म में उन्होंने शहज़ादा सलीम की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक है.
गंगा जमुना (1961): – इस फिल्म में उन्होंने एक किसान की भूमिका निभाई और इसे खूब सराहा गया.
दिलीप कुमार के अभिनय की विशेषता उनकी स्वाभाविकता और गहराई थी. वे अपने पात्रों में पूरी तरह से ढल जाते थे और उनकी हर भूमिका में जीवन का संचार करते थे. उन्होंने ट्रैजेडी रोल्स के साथ-साथ कॉमेडी और रोमांटिक रोल्स में भी सफलता पाई. दिलीप कुमार ने 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जो एक रिकॉर्ड है. उन्हें वर्ष 1994 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया. उन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.
दिलीप कुमार ने वर्ष 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह किया. उनकी जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री में एक आदर्श जोड़ी माना जाता है. दिलीप कुमार ने अपने जीवनकाल में कई सामाजिक और चैरिटी के कार्यों में हिस्सा लिया और समाज सेवा में भी योगदान दिया. दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ. उनकी मृत्यु से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी यादें और फिल्में सदैव जीवित रहेंगी.
दिलीप कुमार का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और उनकी अभिनय कला, फिल्मों और योगदान को सदैव याद किया जाएगा.