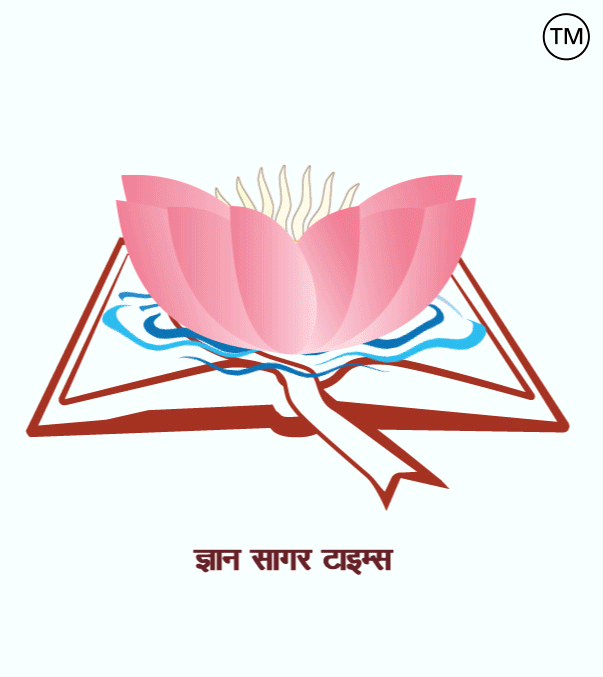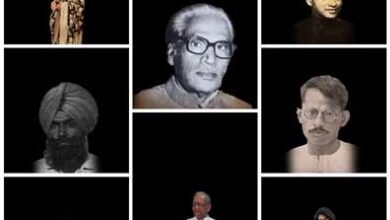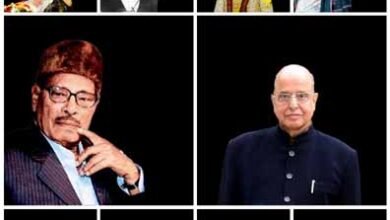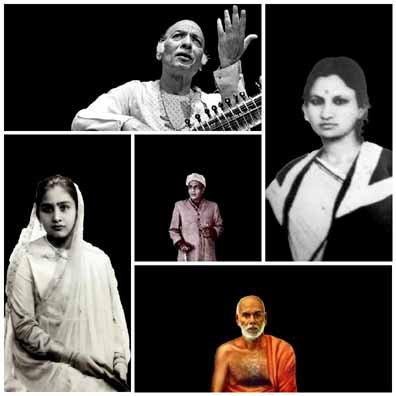
व्यक्ति विशेष -610.
संत श्री नारायण गुरु
संत श्री नारायण गुरु एक महान समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे, जिन्होंने केरल, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनका जन्म 20 अगुस्त 1855 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के चेम्पाझन्थी नामक गांव में हुआ था. वे एक निम्न जाति (एझावा) से थे, जो उस समय सामाजिक और धार्मिक रूप से शोषित थी. नारायण गुरु ने अपने जीवन को सामाजिक समानता, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और आत्मज्ञान की खोज में समर्पित किया.
नारायण गुरु ने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि “एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है, मानवता के लिए” (ओरु जाति, ओरु मथम, ओरु दैवम, मानवम). यह उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण है, जो सभी मनुष्यों की समानता और धार्मिक एकता का प्रतीक है. नारायण गुरु ने उन जातियों के लिए मंदिरों का निर्माण किया, जिन्हें उस समय के मुख्य हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने वर्ष 1888 में शिव का एक मंदिर अरुविपुरम में स्थापित किया, जिससे जाति आधारित धार्मिक प्रतिबंधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. यह मंदिर उनके सुधार आंदोलनों का प्रतीक बन गया.
नारायण गुरु ने शिक्षा के महत्व को समझा और कहा कि शिक्षा ही वह साधन है, जिसके द्वारा समाज के पिछड़े वर्ग अपनी स्थिति सुधार सकते हैं. उन्होंने शिक्षा को जाति और धार्मिक भेदभाव से ऊपर रखा और सभी के लिए इसे सुलभ बनाने का प्रयास किया. वे एक महान दार्शनिक और कवि भी थे. उन्होंने मलयालम, संस्कृत, और तमिल भाषाओं में कई कविताएँ और भक्ति रचनाएँ लिखीं. उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता, वेदांत और समाज सुधार के संदेश होते हैं.
नारायण गुरु ने केवल धार्मिक सुधारों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे समाज के आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए भी काम करते रहे. उन्होंने एक अधिक समतावादी और प्रगतिशील समाज की कल्पना की. संत नारायण गुरु का योगदान केवल केरल या दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा. वे पूरे भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रतीक बने. उनके विचार और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और कई संगठनों और आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो समानता और मानवता के लिए कार्य करते हैं. नारायण गुरु की शिक्षाओं ने समाज के सबसे निचले तबकों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत के महान समाज सुधारकों में एक अद्वितीय स्थान दिया. नारायण गुरु का निधन 20 सितम्बर 1928 को हुआ था.
========== ========= ===========
उर्दू शायर फ़िराक़ गोरखपुरी
फ़िराक़ गोरखपुरी, जिनका असली नाम रघुपति सहाय था, उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध शायरों में से एक थे. वे 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और उन्होंने उर्दू शायरी में अपनी अनूठी शैली और गहरी फिलॉसफिकल अंतर्दृष्टि के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की. फ़िराक़ ने अपने शायरी में प्रेम, नैतिकता, और सामाजिक मुद्दों को स्पर्श किया और उनकी रचनाएँ उर्दू साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं.
फ़िराक़ गोरखपुरी ने अपने लेखन में जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया, जिसमें व्यक्तिगत अनुभवों से लेकर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान तक शामिल हैं. उनकी शायरी में गहरी मानवीय संवेदनाएँ और फिलॉसफिकल गहराई दिखाई देती है. फ़िराक़ ने अपने शैक्षिक जीवन में भी उल्लेखनीय योगदान दिया. वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे. उनकी शिक्षा और व्यावसायिक जीवन ने उनकी लेखनी को भी प्रभावित किया.
फ़िराक़ गोरखपुरी को उनके लेखन के लिए कई पुरस्कारों से नवाज़ा गया, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण शामिल हैं. उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों में ‘गुल-ए-नग़मा’, ‘रूबाइयात-ए-फ़िराक़’, और ‘शबिस्तान-ए-वजूद’ शामिल हैं. उनकी शायरी उर्दू साहित्य में उनकी अमर उपस्थिति को सुनिश्चित करती है और आज भी उनकी रचनाएँ उर्दू शायरी के प्रेमियों द्वारा पढ़ी और सराही जाती हैं. फ़िराक़ गोरखपुरी का निधन 3 मार्च, 1892 को हुआ था.
========== ========= ===========
पंत की मानस पुत्री सरस्वती प्रसाद
पंत की मानस पुत्री सरस्वती प्रसाद एक प्रमुख हिंदी साहित्यिक व्यक्तित्व हैं, जो कि कवि महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता “सरस्वती” के संदर्भ में उल्लेखित होती हैं. यह कविता महादेवी वर्मा की काव्य कृति “सप्तपर्णा” में शामिल है. सरस्वती प्रसाद का जन्म 28 अगस्त, 1932 को आरा (बिहार) में हुआ था और उनका निधन 19 सितम्बर, 2013 को हुआ. सरस्वती प्रसाद के पति का नाम रामचन्द्र प्रसाद है.
महादेवी वर्मा ने “सरस्वती” के माध्यम से एक दिव्य और प्रेरणादायक रूप में सरस्वती देवी की पूजा की है, जो ज्ञान, कला, और संगीत की देवी मानी जाती हैं. यह कविता उनकी व्यक्तिगत संवेदनाओं और आध्यात्मिक जुड़ाव को प्रकट करती है, जो साहित्य और कला में गहरी अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का स्रोत बनती है.
पंत की मानस पुत्री नाम से साहित्यिक संदर्भ में सरस्वती प्रसाद को महादेवी वर्मा की महानता और उनकी काव्यात्मक कृतियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.
========== ========= ===========
पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान
आबिदा सुल्तान भोपाल रियासत की राजकुमारी थीं. आबिदा सुल्तान को भारत की पहली महिला पायलट होने का गौरव प्राप्त था. उन्हें 25 जनवरी, 1942 को उड़ान लाइसेंस मिला था. आबिदा सुल्तान मूल रूप से भोपाल की राजकुमारी थीं और भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं.
आबिदा सुल्तान का जन्म 28 अगस्त 1913 को हुआ था. इनके पिता हमीदुल्लाह ख़ान भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे. आबिदा अपने पिता की बड़ी संतान थी. उनकी परवरिश दादी सुल्तान जहां बेगम ने किया था. अपनी दादी के अनुशासन में रहकर बहुत कम उम्र में ही आबिदा सुल्तान कार ड्राइविंग के अलावा घोड़े, पालतू चीतल जैसे जानवरों की सवारी और शूटिंग कौशल में पारंगत हो चुकी थी. उस जमाने में वे बगैर नकाब के कार चलाती थीं.
आबिदा का निकाह 18 जून 1926 को कुरवाई के नवाब सरवर अली ख़ान के साथ हुआ. दादी की प्रिय पोती आबिदा पहली बार पिता के उत्तराधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनी दादी नवाब सुल्तान जहां बेगम के साथ वर्ष 1926 में लंदन गईं थीं. उनका जीवन बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण रहा है. आबिदा सुल्तान ने न केवल पायलट के रूप में काम किया, बल्कि वे खेलों में भी सक्रिय थीं, विशेष रूप से शूटिंग और घुड़सवारी में. भारत के विभाजन के बाद, वह पाकिस्तान चली गईं और वहां उन्होंने अपने शेष जीवन को समर्पित किया. उन्होंने पाकिस्तान में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाएँ निभाईं और पाकिस्तान के लिए भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा.
आबिदा सुल्तान का निधन 11 मई 2002 को हुआ था. उनका जीवन उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और बदलाव के प्रति उनके साहसिक निर्णयों का प्रमाण है.
========== ========= ===========
सितार वादक विलायत ख़ाँ
उस्ताद विलायत खाँ, जिनका जन्म 28 अगस्त, 1928 को गौरीपुर, बांग्लादेश में हुआ था, भारतीय संगीत जगत में एक प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं. उनके पिता उस्ताद इनायत हुसैन ख़ाँ भी एक प्रख्यात सितार वादक थे. विलायत ख़ाँ ने अपनी संगीत शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की और उनकी मृत्यु के बाद उनके चाचा और अन्य पारिवारिक सदस्यों से संगीत की शिक्षा जारी रखी.
उस्ताद विलायत ख़ाँ ने सितार वादन में अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की, जिसे ‘गायकी शैली’ कहा जाता है. उन्होंने अपनी वादन शैली में गायकी की बारीकियों को समाविष्ट किया, जिससे उनका संगीत और भी गहरा और भावपूर्ण बन गया. उनकी इस विशेषता ने उन्हें संगीत जगत में एक अलग पहचान दिलाई.
विलायत खाँ ने अपने जीवन में दो शादियाँ कीं और उनके दोनों बेटे सुजात हुसैन ख़ाँ और हिदायत ख़ाँ भी प्रसिद्ध सितार वादक बने. उन्होंने अपनी शैली को और विकसित किया और अपने प्रदर्शनों में अक्सर गायन भी शामिल किया. उनके योगदान के सम्मान में उन्हें ‘आफताब-ए-सितार’ का सम्मान दिया गया था.
विलायत ख़ाँ की आलोचनात्मक सोच भी उन्हें विशेष बनाती है. उन्होंने भारतीय सम्मान प्रणाली और आकाशवाणी के प्रचालन को लेकर कटु आलोचना की. उन्होंने पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान भी ठुकरा दिए थे, क्योंकि वे मानते थे कि भारत सरकार ने उनके संगीत में योगदान को सही तरीके से सम्मानित नहीं किया. उन्होंने अपने जीवनकाल में केवल ‘आफताब-ए-सितार’ सम्मान को स्वीकार किया था.
उस्ताद विलायत खाँ का निधन 13 मार्च, 2004 को मुंबई में फेफड़ों के कैंसर के कारण हुआ था. उनकी मृत्यु के समय वे 75 वर्ष के थे. उनका अंतिम संस्कार कोलकाता में किया गया था, जहाँ वे अधिकतर अपने जीवन का समय बिताते थे.