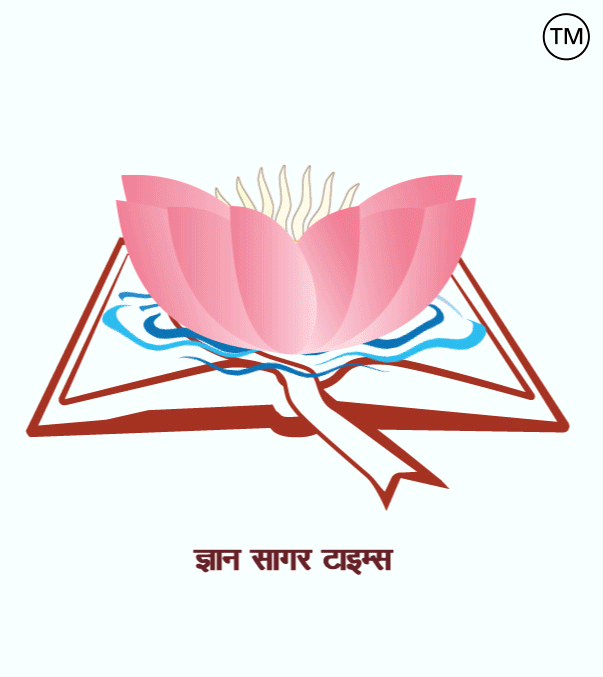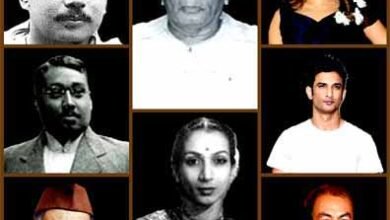संत चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य महाप्रभु भक्तिकाल के महान संत, समाज सुधारक और वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक थे। वे भगवान श्रीकृष्ण के भक्त और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं. उन्हें श्रीकृष्ण का अवतार भी माना जाता है, विशेष रूप से “गौरांग” या “गौर हरि” के नाम से प्रसिद्ध हैं.
चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फ़रवरी 1486 को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप (नादिया) नामक उस गांव में हुआ था. जिसे अब ‘मायापुर’ कहा जाता है. इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था. चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर था, परंतु सभी इन्हें ‘निमाई’ कहकर पुकारते थे. निमाई (चैतन्य महाप्रभु) बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न और अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक थे. 15-16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ था. वर्ष 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई, इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राजपंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ था.
वर्ष 1509 में पिता का श्राद्ध करने निमाई बिहार के गया नगर में गए, तब वहां इनकी मुलाक़ात ईश्वरपुरी नामक संत से हुई. चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन को सबसे प्रभावी भक्ति साधना बताया. उन्होंने महामंत्र का प्रचार किया.
“हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे |
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे ||”
चैतन्य महाप्रभु की मुख्य शिक्षाओं में उन्होंने बताया कि, ईश्वर का नाम जपना ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है. सभी जीव ईश्वर के अंश हैं और सभी के प्रति प्रेम रखना चाहिए. उन्होंने बताया कि, श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार भक्ति मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी.उन्होंने बताया कि, गुरु के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं साथ ही उन्होंने बताया कि, भक्त को भगवान की सेवा में अपने आपको समर्पित कर देना चाहिए.
चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव भक्ति आंदोलन को गति देने के लिए बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया साथ ही वृंदावन की यात्रा कर कई लुप्त कृष्ण लीलास्थलों की पुनर्स्थापना की. उन्होंने गौड़ीय वैष्णव मत की नींव रखी, जिससे आगे जाकर इस्कॉन जैसी संस्थाएं बनीं. उनके प्रमुख शिष्यों में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य आदि प्रमुख थे, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव मत को आगे बढ़ाया. चैतन्य महाप्रभु का निधन 14 जून 1534 को पूरी में हुआ था.
चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को एक सरल और प्रभावी मार्ग बताया, जिसमें जात-पात, धन-वैभव आदि का कोई भेदभाव नहीं था. उन्होंने समाज को प्रेम, करुणा और हरिनाम संकीर्तन का संदेश दिया, जो आज भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा और इस्कॉन जैसे संगठनों के माध्यम से जीवित है.
========== ========= ===========
स्वतंत्रता सेनानी रफ़ी अहमद क़िदवई
रफ़ी अहमद क़िदवई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, समाज सुधारक और प्रखर राजनीतिज्ञ थे. वे भारत के पहले संचार मंत्री (पोस्ट एंड टेलीग्राफ) भी बने और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
रफ़ी अहमद क़िदवई का जन्म 18 फ़रवरी 1894 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के मसौली नामक स्थान पर हुआ था. उनके पिता एक ज़मींदार और सरकारी अधिकारी थे. रफ़ी अहमद क़िदवई की आरम्भिक शिक्षा बाराबंकी में हुई और अलीगढ़ के ए.एम.ओ. कॉलेज से उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी की. उन्होंने शिक्षा के दौरान ही स्वतंत्रता संग्राम में रुचि लेनी शुरू कर दी थी और महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित हुए.
क़िदवई ने खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया. महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन-जागरण किया. नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों में भाग लेने के कारण जेल गए. भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया और कई बार जेल गए.
आजाद भारत में रफ़ी अहमद क़िदवई ने वर्ष 1952 में नेहरू सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने. उन्होंने भारत में राशन प्रणाली को लागू किया, जिससे गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज मिलने लगा. उन्होंने खाद्य संकट से निपटने के लिए न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लागू की थी. संचार मंत्री रहते हुए उन्होंने, डाक सेवाओं और टेलीग्राफ सिस्टम को सुधारने में अहम भूमिका निभाई.
रफ़ी अहमद क़िदवई का निधन 24 अक्टूबर 1954 को दिल्ली में हुआ था. रफ़ी अहमद क़िदवई अवार्ड उनके सम्मान में स्थापित किया गया है, जिसे साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वालों को दिया जाता है.
========== ========= ===========
संत रामकृष्ण परमहंस देव
रामकृष्ण परमहंस देव एक महान भारतीय संत और धार्मिक गुरु थे, जिन्हें भारतीय आध्यात्मिकता और धर्म के पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल (अब पश्चिम बंगाल) के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था. उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था.
रामकृष्ण परमहंस देव ने अपनी युवावस्था में विभिन्न धार्मिक मार्गों का अनुसरण किया, जैसे कि तांत्रिक, वैष्णव, और ईसाई धर्म के सिद्धांतों का अभ्यास. उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि सभी धर्मों के मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं. उन्होंने स्वयं विभिन्न धर्मों का पालन कर यह अनुभव किया कि सभी धर्मों का सार एक ही है और सभी ईश्वर की प्राप्ति के साधन हैं.
रामकृष्ण परमहंस देव का सबसे प्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने उनके उपदेशों को पश्चिमी देशों में फैलाया. रामकृष्ण परमहंस देव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ध्यान और साधना के माध्यम से अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया और उन्हें ईश्वर की अनुभूति करवाई.
उनके उपदेश सरल, प्रेमपूर्ण, और साधारण भाषा में होते थे, और वे इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर की भक्ति और सेवा के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है. उनके विचार और शिक्षाएँ आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. 16 अगस्त 1886 को संत रामकृष्ण परमहंस देव का निधन गोधूलि वेला में हुआ था.
========== ========= ===========
स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास
जयनारायण व्यास, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे. उनका जन्म 18 फरवरी, 1899 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ था और उनका निधन 14 मार्च, 1963 को नई दिल्ली में हुआ.
व्यास जी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वे विशेष रूप से सामंतशाही और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे. उन्होंने राजस्थान में रियासतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी.
वर्ष 1927 में व्यास जी ‘तरुण राजस्थान’ समाचार पत्र के प्रधान संपादक बने और वर्ष 1936 में ‘अखण्ड भारत’ नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया. उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण कई बार जेल की यात्रा भी की. वर्ष 1948 में वे ‘जोधपुर प्रजामण्डल’ के प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1951- 54 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया. वर्ष 1956-57 तक वे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे.
जयनारायण व्यास की सम्मान में उनकी जन्मस्थली जोधपुर में ‘जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय’ का नाम रखा गया है.
========== ========= ===========
कवियित्री कृष्णा सोबती
कृष्णा सोबती एक प्रसिद्ध हिंदी कवियित्री, उपन्यासकार, और कहानीकार थीं, जिन्होंने भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, पाकिस्तान में हुआ था, और उनका निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ. कृष्णा सोबती को उनकी बोल्ड और रियलिस्टिक कहानियों के लिए जाना जाता है, जिनमें समाज में महिलाओं की स्थिति, विभाजन के प्रभाव, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय प्रमुख रूप से उठाए गए हैं.
उनकी प्रमुख कृतियों में ‘मित्रो मरजानी’, ‘दार से बिछुड़ी’, ‘जिंदगीनामा’, और ‘दिलो दानिश’ शामिल हैं. ‘मित्रो मरजानी’ एक ऐसी महिला की कहानी है जो समाज की पारंपरिक बंधनों को तोड़ती है और अपनी यौन इच्छाओं को स्वीकार करती है. ‘जिंदगीनामा’ में, सोबती ने पंजाब के ग्रामीण जीवन का विस्तृत चित्रण किया है.
कृष्णा सोबती को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार (1980), साहित्य अकादमी फैलोशिप (1996), और ज्ञानपीठ पुरस्कार (2017) शामिल हैं. वे अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं और विषयों पर प्रकाश डालती रहीं, जिससे वे हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं.
========== ========= ===========
संगीतकार ख़य्याम
संगीतकार ख़य्याम, जिनका असली नाम मोहम्मद जहूर ख़य्याम हाशमी था, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित संगीतकारों में से एक थे. उनका जन्म 18 फरवरी 1927 को राहों (जो अब पंजाब, भारत में है) में हुआ था, और उनका निधन 19 अगस्त 2019 को हुआ. ख़य्याम ने अपने संगीतकार कैरियर में कई यादगार और अमर गीतों की रचना की, जिन्हें उनके सूक्ष्म, भावपूर्ण और शास्त्रीय संगीत प्रभावों के लिए सराहा जाता है.
ख़य्याम के संगीत की विशेषता उनकी अद्वितीय शैली थी, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय भारतीय संगीत के साथ-साथ घजल, भजन, और लोक संगीत को भी समाविष्ट किया. उन्होंने फिल्मों में अपने संगीत के माध्यम से गहराई और भावनाओं को जोड़ा, जिससे उनकी धुनें सिनेमाई परिदृश्यों के साथ गहराई से जुड़ जाती थीं.
उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध कामों में “कभी कभी” (1976), “उमराव जान” (1981), और “बाजार” (1982) शामिल हैं. “उमराव जान” के लिए उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार दोनों प्राप्त किए. उनके संगीत ने न केवल उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई बल्कि व्यापक जन-समर्थन भी प्राप्त किया.
ख़य्याम के संगीत में एक विशिष्ट शैलीगत विविधता और सूक्ष्मता होती थी, जिसने उन्हें अपने समय के अन्य संगीतकारों से अलग किया. उन्हें उनके योगदान के लिए 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. उनका संगीत आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा के महान संगीतकारों में से एक के रूप में याद करता है.
========== ========= ===========
अभिनेत्री निम्मी
अभिनेत्री निम्मी भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं, जिन्होंने वर्ष 1940- 50 के दशक में अपने अभिनय से बहुत नाम कमाया. उनका असली नाम नवाब बानू था, लेकिन फिल्म जगत में उन्होंने निम्मी के नाम से ख्याति प्राप्त की. निम्मी का जन्म 18 फरवरी 1933 को हुआ था.
निम्मी ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1949 में फिल्म ‘बरसात’ से की, जिसमें उन्होंने एक पहाड़ी लड़की की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और इसके बाद वे बहुत से हिट फिल्मों में दिखाई दीं. उन्होंने ‘दीदार’, ‘आन’, ‘उड़न खटोला’, ‘कुंदन’, ‘मेरे मेहबूब’ और ‘पूजा के फूल’ जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
निम्मी को उनकी आँखों के अभिव्यक्ति और गहरी भावनात्मक अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती थी. उनका अभिनय उस समय के दर्शकों को बहुत भावुक और यथार्थवादी लगा. उनके अभिनय में एक खास प्रकार की मासूमियत और गर्मजोशी थी, जिसने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई. निम्मी की फिल्मों और उनकी अभिनय शैली ने उन्हें भारतीय सिनेमा की एक अमर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया है. अभिनेत्री निम्मी का निधन 25 मार्च 2020 को हुआ था.
========== ========= ===========
अभिनेत्री नलिनी जयवंत
नलिनी जयवंत भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 1940 – 50 के दशक में अपने अभिनय के लिए व्यापक पहचान प्राप्त की थी. उनका जन्म 18 फ़रवरी 1926 को हुआ था और उनका निधन 22 दिसंबर 2010 को हुआ. नलिनी जयवंत ने अपने कैरियर की शुरुआत बहनें (1941) और अनोखा प्यार (1948) जैसी फिल्मों से की थी और उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया. उन्हें उनकी खूबसूरती और प्रभावशाली अभिनय कौशल के लिए याद किया जाता है.
नलिनी जयवंत ने “बहेन” (1941), “अनोखा प्यार” (1948), “आरजू” (1950), “रेलवे प्लेटफार्म” (1955), और “काला पानी” (1958) जैसी कई प्रमुख फिल्मों में अभिनय किया. उन्हें अपने समय के सबसे विशिष्ट अभिनेताओं में से एक माना जाता था.
उनका अभिनय कैरियर उस समय के सिनेमा में उनकी विशेष पहचान बनाने में सफल रहा और वे अपने समय की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री बनीं. उनके काम ने उन्हें कई पीढ़ियों के दर्शकों के बीच एक सम्मानित स्थान दिलाया.
========== ========= ===========
अभिनेत्री जिया मानेक
जिया मानेक एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जिन्हें मुख्य रूप से उनके द्वारा निभाई गई दो प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है: ‘गोपी आहूजा’ स्टार प्लस के लोकप्रिय धारावाहिक “साथ निभाना साथिया” में और ‘जीनी’ सब टीवी के शो “जीनी और जूजू” में. जिया मानेक का जन्म 18 फरवरी 1986 को अहमदाबाद में हुआ था.
“साथ निभाना साथिया” में उनके किरदार गोपी को एक सरल, सीधी-सादी और संस्कारी बहू के रूप में दिखाया गया था, जो अपने परिवार की भलाई और खुशी के लिए हमेशा तत्पर रहती है. इस भूमिका के लिए जिया मानेक को व्यापक पहचान और प्रशंसा मिली, और वह घर-घर में लोकप्रिय हो गईं.
“जीनी और जूजू” में उन्होंने एक जादुई जीनी का किरदार निभाया, जो एक अलग तरह की कॉमेडी और मनोरंजन प्रदान करती है. इस भूमिका में भी उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया.
जिया मानेक के अभिनय कौशल और उनकी भूमिकाओं ने उन्हें टेलीविजन उद्योग में एक पहचान दिलाई है, और वह छोटे पर्दे की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं. उनकी भूमिकाएं और उनका काम विभिन्न दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहा है, जिससे उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है.
========== ========= ===========
तैमूर लंग
तैमूर लंग, जिन्हें तैमूर और तमरलेन के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान मध्य एशिया में एक महान तुर्क-मंगोल विजेता और साम्राज्य के संस्थापक थे. उनका जन्म 8 अप्रैल 1336 को शहरिसब्ज, आज के उज्बेकिस्तान में हुआ था, और उनका निधन 18 फरवरी 1405 को हुआ था. तैमूर को इतिहास में एक क्रूर विजेता के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने जीवनकाल में एशिया के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की.
तैमूर का उदय 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ, और उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जो मध्य एशिया, ईरान, आधुनिक अफगानिस्तान, और कुछ हद तक भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला था. उन्होंने अपनी सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने विरोधियों के खिलाफ निर्ममता का प्रदर्शन किया, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई.
तैमूर का उद्देश्य मंगोल साम्राज्य की पुनः स्थापना करना था, जिसे चंगेज खान ने स्थापित किया था. उन्होंने खुद को चंगेज खान का वंशज मानते हुए अपनी विजयों को उसी का विस्तार माना. उनकी मृत्यु के बाद, उनके वंशजों ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने बाद में भारत पर शासन किया.
तैमूर के शासन और विजय अभियानों ने उस समय के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला. उनके कार्यों ने कई क्षेत्रों में विनाश और पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणामस्वरूप कला, वास्तुकला, और सांस्कृतिक विकास में नई दिशाएँ मिलीं.