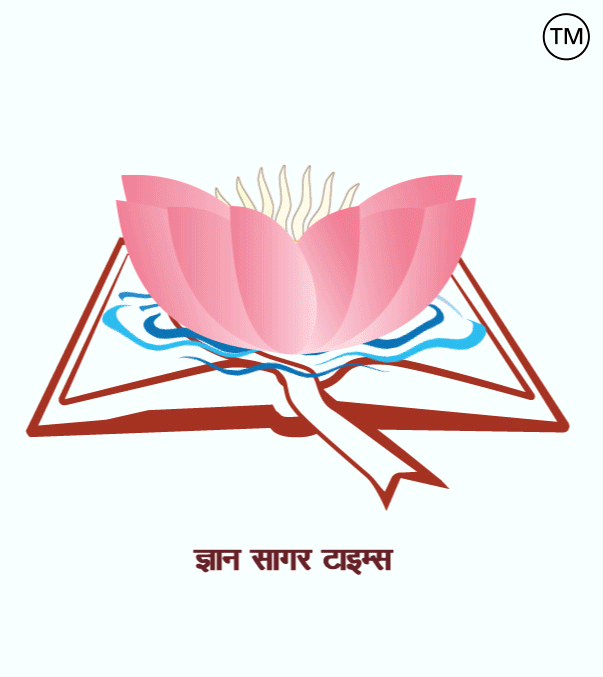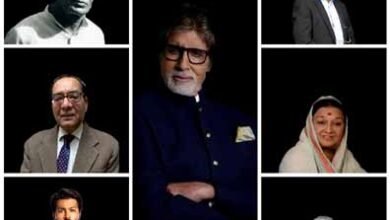स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राय भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता थे. उन्हें “पंजाब केसरी” (पंजाब का शेर) और “लाल-बाल-पाल” त्रिमूर्ति (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल) के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है. ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध थे.
लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुड़ीके गाँव (अब पंजाब, भारत) में हुआ था. उनके पिता राधा कृष्ण आज़ाद एक अध्यापक और उर्दू व फारसी के विद्वान थे. लाला लाजपत राय ने अपनी शिक्षा लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की और वकालत की पढ़ाई की.
लाजपत राय ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय वस्त्रों को अपनाने व विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की अपील की. साइमन कमीशन भारतीयों की राय के बिना भारत में संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव लेकर आया था। लाला लाजपत राय ने इसका जोरदार विरोध किया. 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया. उनकी चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया.
वे आर्य समाज के प्रबल समर्थक थे और दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित थे. उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, जातिवाद के खिलाफ जागरूकता, और दीन-हीन लोगों की सेवा के लिए कई कदम उठाए. उन्होंने “दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) कॉलेज” की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने “पंजाब नेशनल बैंक” और “लक्ष्मी बीमा कंपनी” की स्थापना में योगदान दिया.
लाला लाजपत राय ने कई किताबें लिखीं, जिनमें “यंग इंडिया”, “द स्टोरी ऑफ माय डेपोर्टेशन”, और “अनहैप्पी इंडिया” प्रमुख हैं. लाला लाजपत राय का बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना. उनके बलिदान ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए जॉन सॉन्डर्स की हत्या की. उनके नाम पर भारत में कई शैक्षणिक संस्थान, सड़कें, और सार्वजनिक स्थल बनाए गए हैं.
लाला लाजपत राय का जीवन त्याग, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है. उनका बलिदान भारत के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा.
========== ========= ===========
‘प्रथम आर्मी कमाण्डर इन चीफ़’ के.एम. करिअप्पा
के.एम. करिअप्पा, जिन्हें फील्ड मार्शल कोडंडेरा मदप्पा करिअप्पा के नाम से भी जाना जाता है. वो भारतीय सेना के प्रथम कमांडर-इन-चीफ थे. उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक में हुआ था, और उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दीं और बाद में आजाद भारत की सेना के पहले प्रमुख बने.
करिअप्पा ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली और वे 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बने. उनके कार्यकाल में, उन्होंने विशेष रूप से कश्मीर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सेना की रीस्ट्रक्चरिंग और पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया.
करिअप्पा ने अपने दृढ़ नेतृत्व और सख्त अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे. उन्होंने सेना में उच्च स्तरीय प्रोफेशनलिज्म और ईमानदारी को बढ़ावा दिया और सैन्य बलों में जातिवाद और क्षेत्रीयता को खत्म करने के लिए कड़े प्रयास किए.
उनके योगदान के सम्मान में, भारत सरकार ने उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया. के.एम. करिअप्पा का निधन 15 मई 1993 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत और सेना के प्रति उनके असाधारण योगदान आज भी भारतीय सेना और देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं.
========== ========= ===========
साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र
विद्यानिवास मिश्र हिंदी और संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, विद्वान और संपादक थे. उनका 28 जनवरी 1926 को पकडडीहा गाँव, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ था. मिश्र ने हिंदी साहित्य में अपने गहन ज्ञान और संस्कृति के प्रति गहरी समझ के लिए व्यापक पहचान बनाई. उन्होंने न केवल साहित्यिक कृतियों का सृजन किया बल्कि साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया और भारतीय संस्कृति व दर्शन पर गहराई से लिखा.
विद्यानिवास मिश्र ने विविध विषयों पर लिखा, जिसमें कविता, आलोचना, यात्रा वृतांत, और निबंध शामिल हैं. उनकी लेखन शैली में गहराई, व्यंग्य और विचारों की प्रखरता स्पष्ट दिखाई देती है. उन्होंने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए.
मिश्र की कुछ प्रमुख कृतियों में “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे”, “काशी की अस्सी”, “गंगा जमुनी तहज़ीब” और “कृष्ण की अत्मकथा” शामिल हैं. उनकी रचनाएं न केवल हिंदी साहित्य में उनके योगदान को दर्शाती हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रति उनकी गहरी समझ और अनुराग को भी प्रकट करती हैं.
विद्यानिवास मिश्र का निधन 14 फ़रवरी 2005 को हुआ था. उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया. उनकी गहन अंतर्दृष्टि और विचारशील लेखन ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक अमूल्य रत्न के रूप में स्थापित किया. उनके निधन के बावजूद, उनकी कृतियाँ और विचार आज भी साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन में प्रासंगिक हैं.
========== ========= ===========
गायक पंडित जसराज
पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक और मेवाती घराने के प्रतिनिधि थे. उनकी आवाज़, संगीत में गहराई, और भक्ति से ओत-प्रोत गायकी ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक अनूठी पहचान दी. वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायकों में से एक माने जाते हैं.
पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार, हरियाणा में हुआ था. उनके पिता पंडित मोतीराम भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, लेकिन पंडित जसराज जब केवल चार वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया. उनका परिवार मेवाती घराने से संबंधित था, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है.
जसराज ने अपने बड़े भाई पंडित मणिराम से संगीत की शिक्षा प्राप्त की. शुरुआत में उन्होंने तबला वादक बनने की इच्छा रखी, लेकिन बाद में शास्त्रीय गायन में रुचि बढ़ी और उन्होंने इसे ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया. उनकी गायकी पर भक्ति रस और खयाल गायन का गहरा प्रभाव था.
पंडित जसराज ने खयाल गायकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनकी गायकी में भक्ति रस और रागों की गहराई के साथ भावनात्मक अभिव्यक्ति की अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है.उन्होंने ठुमरी, भजन, और हवेली संगीत (जो कृष्ण भक्ति से जुड़ा है) में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने ‘जसरंगी जुगलबंदी’ नामक गायकी शैली की शुरुआत की, जिसमें एक पुरुष और महिला गायक अलग-अलग रागों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी धुनें एक-दूसरे के साथ मेल खाती हैं. यह शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक अनूठा प्रयोग मानी जाती है.
पंडित जसराज के भजन, जैसे ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ और ‘मेरो आला बाल गोपाल’, अत्यंत लोकप्रिय हैं. उनकी गायकी में अध्यात्म और संगीत का अद्भुत संगम था, जिसने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया. पंडित जसराज को भारत सरकार द्वारा उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जिनमें – पद्म विभूषण (2000), पद्म भूषण (1990), पद्म श्री (1975), अमेरिका में 2019 में, एक ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया—पंडितजसराज ग्रह, उन्हें भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट भी प्राप्त हुई.
पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था. उनके निधन से भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपूरणीय क्षति हुई, लेकिन उनकी संगीत विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. पंडित जसराज भारतीय संगीत की एक ऐसी विभूति थे, जिन्होंने अपने संगीत के जरिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया.
========== ========= ===========
पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर
सुमन कल्याणपुर भारतीय सिनेमा की मशहूर पार्श्व गायिका हैं, जिनकी आवाज़ को अक्सर लता मंगेशकर की आवाज़ के समान माना जाता है. उनके मधुर और भावपूर्ण गीतों ने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग (वर्ष 1950-70) में श्रोताओं का दिल जीत लिया. सुमन कल्याणपुर का नाम उस समय के सबसे प्रतिभाशाली गायकों में गिना जाता है.
सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को धाका, बांग्लादेश (तत्कालीन भारत) में हुआ था. उनका परिवार बाद में मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) आकर बस गया. उन्होंने बचपन से ही संगीत में रुचि दिखाई और संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की.
सुमन कल्याणपुर ने वर्ष 1954 में फिल्म ‘मंगला’ से अपना पार्श्व गायन में कैरियर शुरू की थी. उनकी पहली बड़ी सफलता वर्ष 1955 की फिल्म ‘दरवाजा’ के गाने से आई. इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में सैकड़ों गाने गाए और खुद को एक प्रमुख गायिका के रूप में स्थापित किया.
सुमन की आवाज़ को बेहद मीठा और कोमल माना जाता है. उनकी गायकी में सरलता और गहराई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, देशभक्ति, और दुखभरे गीतों में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी. सुमन कल्याणपुर के कई गाने सदाबहार माने जाते हैं.
लोकप्रिय गाने: –
न तुम हमें जानो (फिल्म: बात एक रात की, 1962)
मेरा दिल जो मेरा होता (फिल्म: झुमरू, 1961)
अजब तेरा करम भगवान (फिल्म: कांच की गुड़िया, 1961)
छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा (फिल्म: पायल की झंकार, 1963)
दिल एक मंदिर है (फिल्म: दिल एक मंदिर, 1963)
कभी दिन कभी रात (फिल्म: बदनसूरत, 1963)
आप के पहलू में आकर रो दिए (फिल्म: मेरा साया, 1966)
सुमन कल्याणपुर ने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें एस.डी. बर्मन, शंकर-जयकिशन, मदन मोहन, रोशन, चेतन आनंद, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल शामिल हैं. सुमन कल्याणपुर की आवाज़ और गायन शैली को अक्सर लता मंगेशकर से तुलना की जाती थी. हालांकि, उन्होंने अपनी विशिष्टता बनाए रखी और श्रोताओं को अपनी मधुर आवाज़ से प्रभावित किया.
हालांकि सुमन कल्याणपुर को मुख्यधारा में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी लता मंगेशकर और आशा भोसले को मिली, लेकिन उनके योगदान को कई बार सम्मानित किया गया. सुमन कल्याणपुर का विवाह वर्ष 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से हुआ था. उन्होंने अधिकतर फिल्मों में गाने के बाद वर्ष 1980 के दशक के अंत में फिल्म संगीत से दूरी बना ली और एक शांत जीवन व्यतीत किया. उनकी आवाज़ का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है.
सुमन कल्याणपुर का संगीत भारतीय सिनेमा का एक अनमोल हिस्सा है. उनके गाए हुए गाने आज भी सदाबहार हैं और उनकी आवाज़ ने संगीत प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है. उनका योगदान भारतीय संगीत के स्वर्ण युग को समृद्ध करने में अद्वितीय है.
========== ========= ===========
वैज्ञानिक राजा रमन्ना
राजा रमन्ना भारत के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों में से एक थे. उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक और वर्ष 1974 के पोखरण-1 परमाणु परीक्षण के मुख्य शिल्पकारों में गिना जाता है. उनके वैज्ञानिक योगदान ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
राजा रमन्ना का जन्म 28 जनवरी 1925 को तुमकुर, कर्नाटक में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु में हुई. उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन विश्वविद्यालय गए, जहाँ उन्होंने नाभिकीय भौतिकी (Nuclear Physics) में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की.
राजा रमन्ना ने भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में अत्यधिक योगदान दिया. उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वे होमी भाभा के साथ जुड़े और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर काम किया. वर्ष 1974 के पोखरण-1 परमाणु परीक्षण (Operation Smiling Buddha) में वे मुख्य वैज्ञानिकों में से एक थे. इस परीक्षण ने भारत को दुनिया के चुनिंदा परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल किया.
राजा रमन्ना ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के निदेशक के रूप में कार्य किया.रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में भी उनकी अहम भूमिका रही. वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से भी जुड़े रहे. उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत की. उन्होंने ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा, और कृषि में परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए तकनीकों को विकसित किया.
राजा रमन्ना ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए और नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा दिया. उनके नेतृत्व में भारत ने परमाणु ऊर्जा और सैन्य अनुसंधान के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की. राजा रमन्ना के योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया. जिनमे – पद्म विभूषण (1975), पद्म भूषण (1973), शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार. वे कई वैज्ञानिक संस्थानों के सदस्य रहे और उन्हें वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला.
वैज्ञानिक योगदान के अलावा, राजा रमन्ना ने राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. वे वर्ष 1990 में राज्यसभा (भारत की संसद का उच्च सदन) के सदस्य बने. उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई. राजा रमन्ना बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे.वे संगीत के प्रेमी थे और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि रखते थे. उन्होंने पियानो बजाने में भी महारत हासिल की थी. उनका निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ था.
उनके योगदान ने भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.उनके काम ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को प्रेरणा दी और उनके द्वारा विकसित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत की सुरक्षा और विकास का मजबूत आधार बना. राजा रमन्ना भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने अपने कार्यों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई. उनका जीवन और योगदान भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है.
========== ========= ===========
अभिनेता तथा फ़िल्म निर्माता-निर्देशक सोहराब मोदी
सोहराब मोदी भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता, निर्माता, और निर्देशक थे, जिन्हें ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है. उनका जन्म 2 नवंबर 1897 को बंबई (अब मुंबई) में हुआ था. भारतीय सिनेमा में उन्होंने अपने जीवन में कई यादगार और प्रभावशाली फिल्में बनाईं, जो आज भी सराही जाती हैं.
सोहराब मोदी ने वर्ष 1930 के दशक में फ़िल्म निर्माण में कदम रखा और वर्ष 1935 में अपनी फ़िल्म कंपनी, मिनर्वा मूवीटोन की स्थापना की. उनकी फ़िल्में सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती थीं, और उन्होंने फ़िल्मों में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में सिकंदर (1941), पुकार (1939), प्रिथ्वीराज चौहान (1944), और झाँसी की रानी (1953) जैसी ऐतिहासिक और महाकाव्य फिल्मों के नाम शामिल हैं.
सोहराब मोदी की आवाज़ और संवाद अदायगी का अंदाज बहुत प्रभावशाली था, जिसके कारण वे भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से न्याय, समानता, और देशभक्ति जैसे विषयों को चित्रित किया, जिससे उनके सिनेमा में गहरी संवेदनशीलता और प्रासंगिकता दिखाई देती है.
वर्ष 1953 में रिलीज़ हुई उनकी फ़िल्म झाँसी की रानी भारत की पहली टेक्नीकलर फ़िल्मों में से एक थी, जिससे सोहराब मोदी भारतीय सिनेमा में तकनीकी नवाचार के लिए भी पहचाने जाते हैं. अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। सोहराब मोदी का भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव है, और उन्हें भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक फिल्मों के एक बेमिसाल निर्माता-निर्देशक के रूप में याद किया जाता है. सोहराब मोदी का निधन 28 जनवरी, 1984 को हुआ था.
========== ========= ===========
संगीतकार ओ. पी. नैय्यर
ओ. पी. नैय्यर एक प्रमुख भारतीय संगीतकार थे, जो भारतीय सिनेमा के लिए संगीत बनाने में प्रसिद्ध थे। वह 16 जनवरी 1926 को पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए थे और 28 जनवरी 2007 को दुनिया से चले गए.
ओ. पी. नैय्यर ने अपनी संगीतकारी कैरियर की शुरुआत वर्ष 1952 में की और वे जल्द ही एक प्रमुख संगीतकार बन गए. उन्होंने हिन्दी सिनेमा के लिए कई प्रमुख गीतों की संगीतकारी की, और उनका संगीत आमतौर पर लोकप्रिय था.
ओ. पी. नैय्यर के प्रसिद्ध गीत : – बाबूजी धीरे चलना प्यार में ज़रा संभलना, ये लो मैं हारी पिया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेके पहला पहला प्यार, ये देश है वीर जवानों का, उड़े जब जब ज़ुल्फ़ें तेरीरेशमी सलवार कुर्ता जाली का, इक परदेसी मेरा दिल ले गया.
ओ. पी. नैय्यर का संगीत अक्सर आसान मेलोडीज़ और लोकप्रियता के लिए जाना जाता है, और उनके संगीत में उनकी ख़ास तालमेल और गाने की आवाज़ का महत्वपूर्ण भूमिका थी.