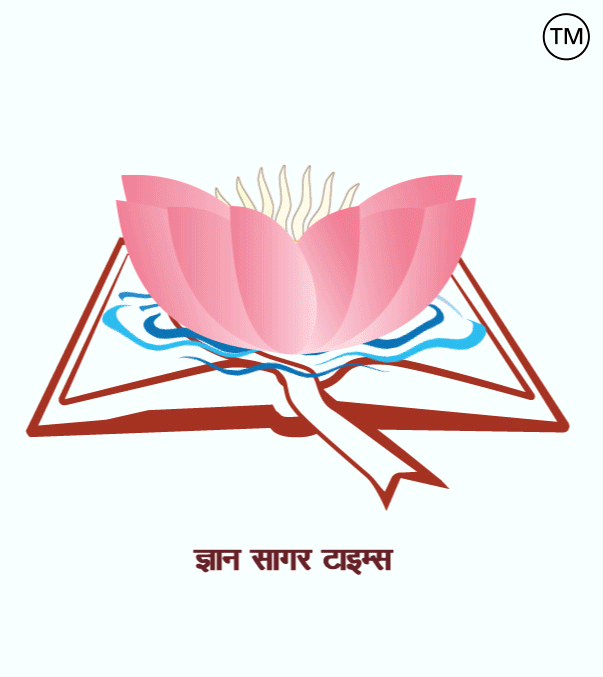धुप-छांव -3.
मैंने प्रभात को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था-किताबों में खोया हुआ, जैसे हर शब्द से वो खुद को जोड़ना चाहता हो. उसे देखकर मुझे अपनी दादी की कही एक बात याद आई- “कुछ लोग धूप में उगते हैं, कुछ छांव में पनपते हैं… पर कुछ, समय के साथ अपने ही मौसम बनाते हैं.”
वह धूप-छांव का मौसम था.
प्रभात जब अपनी कहानियाँ पढ़कर सुनाता, मेरी हँसी उसके शब्दों पर नहीं, उसकी खामोशी पर होती. इतनी कोमलता मैंने बहुत कम देखी थी. पर मैं… मैं तो हमेशा आगे दौड़ने वाली रही. मेरे लिए भावनाएँ एक यात्रा का पड़ाव थीं, मंज़िल नहीं.
मैंने एक बार उससे पूछा, “तुम इतनी परछाइयों में कैसे आराम से रह लेते हो?” उसने मुस्कराकर कहा, “क्योंकि छांव में दिल की धड़कनें साफ़ सुनाई देती हैं.”
उस दिन कुछ टूटा था मेरे भीतर. मैंने जाना कि मैं पूरी धूप में नहीं थी-मैं खुद अपनी छांव से भाग रही थी. मेरे आत्मविश्वास की दीवार पर ज़रा सी नमी आई और उसपर उसकी कहानियों की बेलें चढ़ने लगीं.
प्रभात जब वापस अपने गांव लौट गया-बिना अलविदा कहे, मैंने कई रातें उस एक प्रश्न में बिताईं: “क्या उसे मेरे पास ठहरने के लिए कह सकती थी?”
पर शायद वह किसी की नहीं था-वह तो धूप और छांव के बीच की वह खुली जगह था, जहाँ हवा चलती है. जहाँ कोई भी रुककर खुद से मिल सकता है.
मैंने उसकी आख़िरी लिखी कहानी पढ़ी- “धूप से छांव तक और फिर लौट आना.” उसमें एक पंक्ति थी— “जिसने छांव में मेरा इंतज़ार किया, वही मेरा उजाला बना.”
वो मैं थी… शायद. लौटना, लेकिन किसी और की तलाश में “हम अक्सर उन्हीं रास्तों पर लौटते हैं जहाँ कोई हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा होता, पर उम्मीद रहती है कि कोई मिल जाए.”
शेष भाग अगले अंक में…,